Story
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आधारित दुष्प्रचार कैसे फैलाया जाता है?






ऐसा लगता है कि भारत प्लूटोक्रेसी (धन-तंत्र ) की ओर बढ़ रहा है। जी, आपने सही सुना है। वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक है "बिलेनियर राज इन इंडिया"। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या 1990 के दशक तक गिनी चुनी ही थी और 2022 तक भारत में 160 से ज़्यादा अरबपति मौजूद हैं। विभिन्न डेटा सेटों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत धन-तंत्र की ओर बढ़ रहा है, सरल शब्दों में कहें तो सरकार सीधे या परोक्ष रूप से अमीर या उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों से प्रभावित होकर नीतियां बना रही है।



"चूल्हा पहेली" की जड़ गरीबी, ऊर्जा विकल्प और स्वास्थ्य के बीच अटूट संबंध में निहित है। ग्रामीण आबादी के लिए एलपीजी की वकालत एक समाधान की तरह लग सकती है, लेकिन यह दोहरा बंधन पेश करती है। सबसे पहले, एलपीजी एक जीवाश्म ईंधन है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाता है। दूसरे, जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देने के प्रति वैश्विक घृणा इसे गरीबों के लिए किफायती बनाने में एक चुनौती पैदा करती है।



एक भारतीय महिला होने के नाते, किसने यह पंक्ति नहीं सुनी है? चाहे वह शादी हो, पारिवारिक समारोह हो या फिर अंतिम संस्कार, अविवाहित महिला हर जगह चर्चा का विषय होती है! मैं मेरे समाज से एक सवाल पूछना चाहता हूँ! महिलाओं पर 30 वर्ष की उम्र तक शादी करने और बच्चे पैदा करने का दबाव क्यों डाला जाता है? शादी का वास्तविक अर्थ क्या है। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त सहमति और संविदात्मक संबंध में पति-पत्नी के रूप में एकजुट होने की स्थिति ही विवाह है। यानी की कि इसकी मूल परिभाषा में भी हम देख सकते हैं कि विवाह केवल विवाह करने वाले दो लोगों की इच्छा और निर्णय पर ही केंद्रित होता है। ऐतिहासिक रूप से, शादी पुरुषों का महिलाओं पर स्वामित्व के बारे में रही है। महिलाएं संपत्ति हैं। शादी में महिलाएं एक वस्तु हैं। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से सभी पितृसत्तात्मक प्रथाओं के खिलाफ हूं। लेकिन जब तक ऐसी प्रथाएं ठीक नहीं हो जातीं, मैं शादी के लिए सहमत नहीं हूं। हां, दुख की बात है कि आज भी, 21वीं सदी में, एक महिला की राय को अंतिम प्राथमिकता दी जाती है, भले ही वह उसकी अपनी शादी से संबंधित हो। और ऐसे देश में जहां जाति व्यवस्था अभी भी कायम है, एक लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी अन्य जाति में शादी नहीं कर सकती। उसे उसी धर्म, जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता और संस्कृति से होना चाहिए। यह सूची बहुत लंबी है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी दूसरे से विवाह करके उसके घर की शोभा बढ़ाएं। और अगर कोई अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है , चाहे वह शादी बाद में करना चाहे या न करे, अपने माता-पिता और आस-पास के अन्य लोगों को निराश करने का बोझ उसके सपनों और आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है। मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती जो अपने द्वारा किए गए त्याग के लिए बच्चे को दोषी ठहराए। इससे बेहतर होगा कि मैं अपना या किसी और के जीवन का बलिदान न करूं, ताकि किसी पर यह जिम्मेदारी का बोझ न पड़े। लेकिन पुरुषों पर इस तरह का दबाव वास्तव में नहीं देखा जाता। मुझे लगता है कि महिलाओं पर जल्दी शादी करने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि कहीं न कहीं समाज को यह अहसास है कि महिला जितनी बड़ी होती जाती है, उसे नियंत्रित या मैनुपुलेट नहीं किया जा सकता। महिलाओं पर तीस की उम्र तक शादी करने का दबाव पड़ने का एक और कारण यह है उनका बायलॉजिकल क्लॉक। बायलॉजिकल क्लॉक शब्द का अर्थ है कि 30 उम्र के बाद में गर्भवती होना आम तौर पर कठिन होता है। हाँ, यह सच है कि महिलाओं में मासिक धर्म शुरू होने के साथ ही अंडों की संख्या और गुणवत्ता में कमी आती है। 35 वर्ष की आयु तक प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। हां, युवा होने पर महिलाओं का शरीर शारीरिक रूप से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अन्य कारकों का क्या? उदाहरण के लिए मेंटल, इमोशनल और फाइनेंसियल स्टेबिलिटी। जो लोग 30 के बाद बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए वास्तव में इसके क्या लाभ हैं? एक लाभ यह है कि बच्चों में बेहतर संज्ञानात्मक कौशल होगा और बड़ी उम्र की माताएँ आर्थिक रूप से स्थिर होंगी, उनकी शिक्षा का स्तर अधिक होगा जो इन बच्चों के अधिक बुद्धिमान होने के पीछे एक कारक हो सकता है। टेक्नोलॉजी में प्रगति ने 40 और यहां तक कि 50 वर्ष की आयु में भी महिलाओं के लिए मां बनना संभव बना दिया है। हमेशा याद रखें कि बच्चा पैदा करने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तैयार हों। विवाह एक विकल्प होना चाहिए और जो लोग इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते, उन्हें समाज में बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए। जब परंपरावादी कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है, तो यह विचार कि आपको शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, अब बदल रहा है। समय के साथ लोग बदलते हैं, समय के साथ लोग और उनकी मानसिकता बदलती है। दुनिया बदल रही है। इसलिए समय के साथ हमारे दृष्टिकोण में भी बदलाव आना चाहिए। इसलिए, 21वीं सदी में विवाह की अवधारणा को बदलने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि विवाह एक स्वाभाविक पितृसत्तात्मक संस्था है। यह पुरातन मानसिकता उस समय से उपजी है जब बेटियों को उनके परिवारों के लिए बोझ माना जाता था। वह समय था जब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थीं और इस प्रकार 'बोझ' से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका था कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन समय बदल गया है। आज, महिलाओं के पास शिक्षा तक अधिक पहुंच है, वे किसी भी प्रदाता की आवश्यकता के बिना भावनात्मक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अपने सपनों पूरा कर सकती हैं बावजूद हमें ऐसा क्यों सुनना पड़ता है ? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी महिला को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह विवाह भी अधिक समायोजनशील, लचीले और समावेशी होते जा रहे हैं। फिलहाल, मैं यह स्वीकार करने लगी हूं कि विवाह पूरी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी, यह एक विकल्प है और इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए और इसे तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति अपने बारे में आश्वस्त हो। अगर लोगों पर इतना दबाव न डाला जाए तो वे अपने जीवन को समझने में समय लगाएंगे कि वे कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं, और रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। विवाह एक आजीवन प्रतिबद्धता है और आपको यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि आप कब और किससे विवाह करेंगे। अब समय आ गया है कि हम यह समझें कि किसी महिला की सामाजिक स्थिति का उसकी उंगली में पहनी अंगूठी से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यदि आप एक ऐसी महिला हैं जो शादी के दबाव के कारण दुविधा में हैं, तो कृपया समझें और अपना निर्णय स्वयं करें।



अयोध्या का परिवर्तन: राम मंदिर की छाया में पुनर्जन्म हुआ एक शहर



मैं तेनु फिर मिलंगी किथे? किस तरह? पता नहीं



मेरी दृष्टि में महिला आरक्षण को जातियों में बांटना कहीं से भी उचित नहीं है।: prof चंद्रकला पाडिया

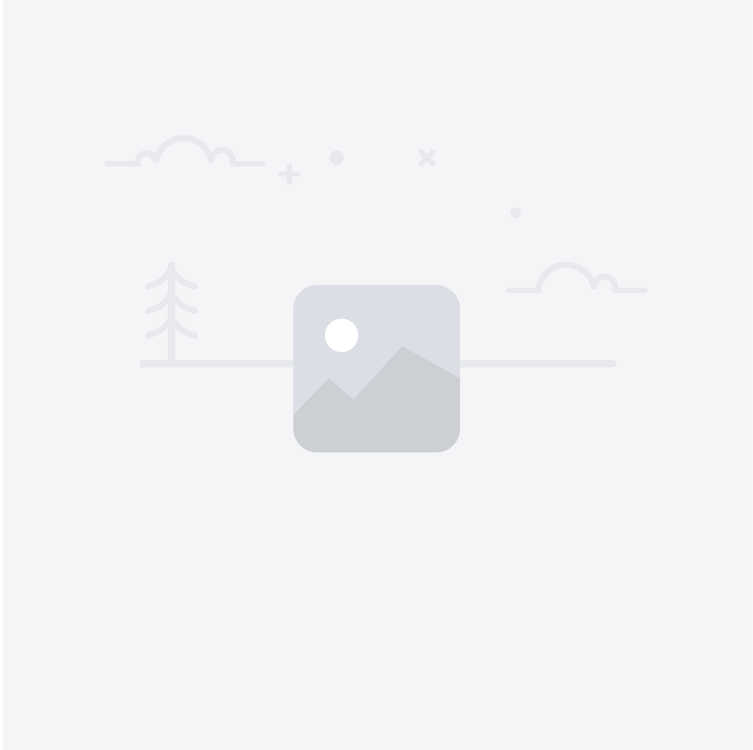
उज्जवला योजना का सच



संविधान दिवस - भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 को डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। आज ही का दिन भारत की नियती में वह महत्वपूर्ण पड़ाव था जब राष्ट्र शिल्पियों के गहन मंथन से तैयार हुए रचना को संविधान के रूप में अंगीकार किया गया । आज हम उसी गौरवशाली क्षण का स्मरण कर रहे हैं। आनंद और उल्लास के साथ ही यह आत्मावलोकन का भी अवसर है। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाना है। उन्हें संविधान की मूल भावना से परिचित कराना और संविधान के प्रति उनकी आस्था को मजबूत करना है । पहली बार संविधान को वास्तव में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया था, जिसके बाद यह जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू हो गया। आज 7वें संविधान दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं कि संविधान क्या है और कैसे यह बनाया गया था। भारत की आजादी से पहले ही बेहतर लोकतंत्र के लिए संविधान बनाने की चर्चा शुरू हो गई थी। साल 1934 में पहली बार कम्युनिस्ट नेता एम-एन रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसके बाद संविधान के गठन पर बहस जारी रही । वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की। जिसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी थी इन सबके बीच 1938 में कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन की घोषणा की। उस दौरान भारत में शामिल मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त भागों में विभाजित किया जाए। जिसमें भारत और पाकिस्तान के देश शामिल थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मुस्लिम लीग की मांगों को खारिज करते हुए, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए जारी केवल 296 सीटों के लिए चुनाव कराया। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 , मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटी पार्टियों को कुल 15 सीटें मिली उस दौरान की देसी रियासतों के लिए सरकार ने 93 सीटें रिजर्व की थी लेकिन रियासतों ने संविधान सभा की बैठक में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया ।काफी दिनों तक चले इस प्रक्रिया के बाद आखिरकार की पहली बार 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई। इसमे 211 सदस्य शामिल थे ।इस सभा में संविधान की संपूर्ण रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई, इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के अलावा सभी नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया। आज़ादी से कुछ महीने पहले 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जिसके बाद 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका काम संविधान का मसौदा तैयार करने के अलावा 1935 में संविधान के लिए एम एन रॉय के निर्देशों पर चर्चा होनी थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर थे। इस कमेटी में अन्य 7 सदस्य भी शामिल थे। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों तक चली संविधान सभा की बैठकों के बाद, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया गया, जिसे आखिरकार 26 नवंबर 1949 को सभी की सहमति से स्वीकार कर लिया गया । बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर, हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा और विविध क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर उचित रूप से गर्व कर सकते हैं। यह हमारे लोगों और हमारे संविधान में हमारे विश्वास की पुष्टि करने का भी समय है क्योंकि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और एक नए आत्मनिर्भर, मजबूत, एकजुट और मानवीय राष्ट्र के अपने सपने को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नए सिरे से समर्पित करते हैं। संविधान लोगों को उतना ही सशक्त बनाता है जितना लोग संविधान को सशक्त करते हैं। निर्माताओं ने महसूस किया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है और कितना विस्तृत है, संस्थानों और लोगों के साथ एक सहजीवी बंधन स्थापित करने में विफल होने पर इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यह संविधान सभा के महापुरुषों की दूरदर्शिता और प्रतिभा ही थी जिसने एक ऐसे संविधान को बनाने में मदद की जिसकी स्वीकार्यता प्रत्येक बीतती पीढ़ी के साथ बढ़ी है। यह देश के आम नागरिक को सलाम करने का भी समय है जिसने संविधान के शब्द और भावना के साथ एक अटूट बंधन स्थापित किया है और हमारी यात्रा के हर कठिन मोड़ पर बुलंदी के प्रति अपने विश्वास और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है।

Write a comment ...